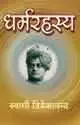|
धर्म एवं दर्शन >> आत्मतत्त्व आत्मतत्त्वस्वामी विवेकानन्द
|
27 पाठक हैं |
आत्मतत्त्व अर्थात् हमारा अपना मूलभूत तत्त्व। स्वामी जी के सरल शब्दों में आत्मतत्त्व की व्याख्या
फिर द्वैतवादी एवं विशिष्टाद्वैतवादी, दोनों यह मानते हैं कि आत्मा स्वभावत: पवित्र है, किन्तु अपने कर्मों से यह अपने को अपवित्र बना लेती है। विशिष्टाद्वैतवादी इसको द्वैतवादियों की अपेक्षा अधिक सुन्दर ढंग से कहते हैं। उनका कहना है कि आत्मा की पवित्रता एवं पूर्णता कभी संकुचित हो जाती है, पर फिर ज्यों की त्यों हो जाती है। और हमारा प्रयास यह है कि उसकी अवस्था को बदलकर पुन: उसकी पूर्णता, पवित्रता एवं शक्ति को स्वाभाविक स्थिति में ले आयें। आत्मा के अनेक गुण हैं, पर उसमें सर्वशक्तिमत्ता या सर्वज्ञता नहीं है। हर पापकर्म उसकी प्रकृति को संकुचित कर देता है और पुण्य कर्म विस्तीर्ण। जिस तरह किसी प्रज्वलित अग्नि से उसी जैसे करोड़ों स्फुलिंग निकलते हैं, उसी तरह इस अपरिमेय सत्ता (ईश्वर) से सभी आत्माएँ निकली हैं। सब का उद्देश्य एक ही है। विशिष्टाद्वैतवादियों का ईश्वर भी सगुण है, पर विशेषता यह है कि वह विश्व की हर चीज में व्याप्त है। वह विश्व की हर वस्तु में हर जगह अन्तर्निहित है। जब शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है, तो उनका तात्पर्य यही रहता है कि ईश्वर सब में व्याप्त है। उदाहरणत: ईश्वर दीवाल नहीं हो जाता, बल्कि वह दीवाल में व्याप्त है। विश्व में कोई ऐसा कण नहीं, ऐसा अणु नहीं, जिसमें वह न हो।
आत्माएँ सीमित हैं; वे सर्वव्यापी नहीं हैं। जब उनकी शक्तियों का विस्तार होता है और वे पूर्ण हो जाती हैं, तो जरामरण के चक्र से मुक्ति पा जाती हैं और सदा के लिए ईश्वर में ही वास करती हैं। अब हम अद्वैतवाद पर आते हैं। मेरे विचार में अब तक विश्व के किसी भी देश में दर्शन एवं धर्म के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसका चरमतम विकास एवं सुन्दरतम पुष्प अद्वैतवाद में है। यहाँ मानव-विचार अपनी अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है और अभेद्य प्रतीत होनेवाले रहस्य से भी पार चला जाता है। यह है अद्वैत वेदान्तवाद। अपनी दुरूहता और अतिशय उत्कृष्टता के कारण यह जनसमुदाय का धर्म नहीं बन पाया।
|
|||||