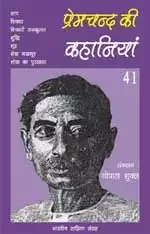|
कहानी संग्रह >> प्रेमचन्द की कहानियाँ 41 प्रेमचन्द की कहानियाँ 41प्रेमचंद
|
146 पाठक हैं |
प्रेमचन्द की सदाबहार कहानियाँ का इकतालीसवाँ भाग
विद्याधरी ने निर्दय होकर कहा- मैंने कुछ नहीं किया, यह उसके कर्मों का फल है।
मैं- तुम्हें छोड़कर और किसकी शरण जाऊँ, क्या तुम इतनी दया न करोगी?
विद्याधरी- मेरे किए अब कुछ नहीं हो सकता।
मैं- देवी, तुम पातिव्रतधारिणी हो, तुम्हारे वाक्य की महिमा अपार है। तुम्हारा क्रोध यदि मनुष्य से पशु बना सकता है, तो क्या तुम्हारी दया पशु से मनुष्य न बना सकेगी?
विद्याधरी- प्रायश्चित करो, इसके अतिरिक्त उद्धार का और कोई उपाय नहीं।
ऐ मुसाफिर, मैं राजपूत की कन्या हूँ। मैंने विद्याधरी से अधिक अनुनय-विनय नहीं की। उसका हृदय दया का आगार था। यदि मैं उसके चरणों पर शीश रख देती, तो कदाचित् उसे मुझ पर दया आ जाती। किन्तु राजपूत-कन्या इतना अपमान नहीं सह सकती। वह घृणा के घाव सह सकती है, क्रोध की अग्नि सह सकती है, पर दया का बोझ उससे नहीं उठाया जाता। मैंने पटरे से उतरकर पतिदेव के चरणों पर सिर झुकाया, और उन्हें साथ लिये हुए घर चली आयी।
कई महीने गुजर गए। मैं पतिदेव की सेवा शुश्रूषा में तन-मन से व्यस्त रहती। यद्यपि उनकी जिह्वा वाणी-विहीन हो गई थी, पर उनकी आकृति से स्पष्ट प्रकट होता था कि वह अपने कर्म से लज्जित थे। रूपांतर हो जाने पर भी उन्हें मांस से अत्यंत घृणा थी। मेरी पशुशाला में सैकड़ों गायें-भैंसे थीं, किन्तु शेरसिंह ने कभी किसी की ओर आँख उठाकर भी न देखा। मैं उन्हें दोनों बेला दूध पिलाती, और संध्या समय उन्हें लेकर पहाड़ियों की सैर कराती। मेरे मन में न जाने क्यों धैर्य और साहस का इतना संचार हो गया था कि मुझे अपनी दशा असह्य न जान पड़ती थी। मुझे निश्चय था कि शीघ्र ही इस विपत्ति का अंत भी होगा।
इन्हीं दिनों हरिद्वार में गंगास्नान का मेला लगा। मेरे नगर के यात्रियों का एक समूह हरिद्वार चला। मैं भी उनके साथ हो ली। दीन-दुखी जनों को दान देने के लिए रुपये और अशर्फियों की थैलियाँ साथ ले लीं। मैं प्रायश्चित करने जा रही थी, इसलिए पैदल ही यात्रा करने का निश्चय कर लिया। लगभग एक महीने में हरिद्वार जा पहुँची। यहाँ भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त से असंख्य यात्री आये हुए थे। संन्यासियों और तपस्वियों की संख्या गृहस्थों से कुछ ही कम होगी। धर्मशालाओं में रहने का स्थान न मिलता था। गंगा-तट पर, पर्वतों की गोद में, मैदानों के वक्षःस्थल पर जहाँ देखिए आदमी-ही-आदमी नजर आते थे। दूर से वे छोटे-छोटे खिलौनों का भाँति दिखाई देते थे। मीलों तक आदमियों का फर्श-सा बिछा हुआ था भजन और कीर्तन की ध्वनि नित्य कानों में आती रहती थी। हृदय में असीम श्रद्धा, गंगा की लहरों की भाँति लहरें मारती थी। वहां का जल, वायु, आकाश शुद्ध था।
|
|||||