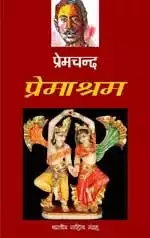|
सदाबहार >> प्रेमाश्रम (उपन्यास) प्रेमाश्रम (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
370 पाठक हैं |
‘प्रेमाश्रम’ भारत के तेज और गहरे होते हुए राष्ट्रीय संघर्षों की पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है
यह कहते-कहते गायत्री फूट-फूट कर रोने लगी। जरा दम लेकर फिर उसी प्रवाह में बोली– श्रद्धा तुम्हें विश्वास न आयेगा, यह मनुष्य पक्का जादूगर है। इसने मुझ पर ऐसा मन्त्र मारा कि मैं अपने को बिलकुल भूल गयी। मैं तुमसे अपनी सफाई नहीं कर रही हूँ। वायुमंडल में नाना प्रकार के रोगाणु उड़ा करते हैं। उनका विष उन्हीं प्राणियों पर असर करता है, जिनमें उसके ग्रहण करने का विकार पहले से मौजूद रहता है। मच्छर के डंक से सबको ताप और जूड़ी नहीं आती। वह बाह्य उत्तेजना केवल भीतर के विकार को उभाड़ देती है। ऐसा न होता तो आज समस्त संसार में एक भी स्वस्थ प्राणी न दिखायी देता। मुझमें यह विकृत पदार्थ था। मुझे अपने आत्मबल पर घमंड था। मैं ऐंद्रिक भोग को तुच्छ समझती थी। इस दुरात्मा ने उसी दीपक से जिससे मेरे अँधेरे घर में उजाला था घर में आग लगा दी, जो तलवार मेरी रक्षा करती थी वही तलवार मेरी गर्दन पर चला दी। अब मैं वही तलवार उसकी गर्दन पर चलाऊँगी। वह समझता होगा कि मैं अबला हूँ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन मैं दिखा दूँगी पानी भी द्रव हो कर भी पहाड़ों को छिन्न-भिन्न कर सकती है। मेरे पूज्य पिता आत्मदर्शी हैं। उन्हें उसकी बुरी नीयत मालूम हो गयी थी इसी कारण उन्होंने मुझे उससे दूर रहने की ताकीद की थी। उन्होंने अवश्य विद्या से यह बात कही होगी। इसीलिए विद्या वहाँ मुझे सचेत करने आयी थी। लेकिन शोक! मैं नशे में ऐसी चूर थी कि पिताजी की चेतावनी की कुछ परवाह न की। इस धूर्त ने मुझे उनकी नजरों में भी गिरा दिया। अब वह मेरा मुँह देखना भी न चाहेंगे।
गायत्री यह कह कर फिर शोकमग्न हो गयी। श्रद्धा की समझ में न आता था कि इसे कैसे सांत्वना दूँ। अकस्मात गायत्री उठ खड़ी हुई। सन्दूक में से कलम, दवात, कागज निकाल लाई और बोली, बहिन, जो कुछ होना था हो चुका इसके लिए जीवन-पर्यन्त रोना है। विद्या देवी थी, उसने अपमान से मर जाना अच्छा समझा। मैं पिशचिनी हूँ, मौत से डरती हूँ। लेकिन अब से यह जीवन त्याग और पश्चात्ताप पर समर्पण होगा। मैं अपनी रियासत से इस्तीफा दे देती हूँ, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। तीन साल से उस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं इतने दिनों तक बिना अधिकार ही उसका उपभोग करती रही। यह रियासत मेरे पतिव्रत-पालन का उपहार थी। यह ऐश्वर्य और सम्पति मुझे इसलिए मिली थी कि कुल-मर्यादा की रक्षा करती रहूँ, मेरी पतिभक्ति अचल रहे। वह मर्यादा कितने महत्त्व की वस्तु होगी जिसकी रक्षा के लिए मुझे करोड़ों की सम्पत्ति प्रदान की गई। लेकिन मैंने उस मर्यादा को भंग कर दिया, उस अमूल्य रत्न को अपनी विलासिता की भेंट कर दिया। अब मेरा उस रियासत पर कोई हक नहीं है। उस घर में पाँव रखने का मुझे स्वत्व नहीं, वहाँ का एक-एक दाना मेरे लिए त्याज्य है। मैं इतने दिनों में हराम के माल पर ऐश करती रही।
यह कह कर गायत्री कुछ लिखने लगी, लेकिन श्रद्धा ने कागज उठा लिया और बोली– खूब सोच-समझ लो, इतना उतावलापन अच्छा नहीं।
गायत्री– खूब सोच लिया है। मैं इसी क्षण ये मँगनी के वस्त्र फेंकूँगी और किसी ऐसे स्थान पर जा बैठूँगी, जहाँ कोई मेरी सूरत न देखे।
|
|||||