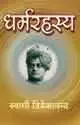|
धर्म एवं दर्शन >> आत्मतत्त्व आत्मतत्त्वस्वामी विवेकानन्द
|
27 पाठक हैं |
आत्मतत्त्व अर्थात् हमारा अपना मूलभूत तत्त्व। स्वामी जी के सरल शब्दों में आत्मतत्त्व की व्याख्या
वेदों में एक अत्यन्त सुन्दर उपमा दी गयी है - वह अनादि पुरुष नि:श्वास के रूप में इस विश्व को प्रकट करता है और श्वासरूप से इसे अपने में अन्तर्निहित करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कि हम एक छोटे से धूलि-कन को साँस के द्वारा निकालते और साँस द्वारा उसे पुन: भीतर ले जाते हैं। यह सब तो बिलकुल ठीक है, लेकिन प्रश्न हो सकता है प्रथम चक्र में इसका क्या रूप था? उत्तर है : प्रथम चक्र से क्या आशय है? वह तो था ही नहीं। यदि तुम काल का प्रारम्भ बतला सकते हो, तो समय की समस्त धारणा ही ध्वस्त हो जाती है। उस सीमा पर विचार करने की चेष्टा करो, जहाँ काल का प्रारम्भ हुआ, तुमको उस सीमा के परे के समय के सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा। जहाँ देश प्रारम्भ होता है, उस पर विचार करो; तुमको उसके परे के देश के सम्बन्ध में भी सोचना पड़ेगा। देश और काल अनन्त हैं, अत: न तो उनका आदि है और न अन्त। ईश्वर ने पाँच मिनट में विश्व की रचना की और फिर वे सो गये और तब से आज तक सो रहे हैं, इस धारणा की अपेक्षा यह उपर्युक्त धारणा कहीं अच्छी है।
दूसरी ओर यह धारणा अनन्त स्रष्टा के रूप में हमें ईश्वर प्रदान करती है। लहरों का एक क्रम है, वे उठती हैं और गिरती हैं और ईश्वर इस अनन्त प्रक्रिया का संचालक है। जिस प्रकार विश्व अनादि और अनन्त है, उसी प्रकार ईश्वर भी। हम देखते हैं कि ऐसा होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम कहें कि किसी समय सृष्टि नहीं थी, सूक्ष्म अथवा स्थूल रूप में भी, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि ईश्वर भी नहीं था, क्योंकि हम ईश्वर को साक्षी, विश्व के द्रष्टा के रूप में समझते हैं। जब विश्व नहीं था, तब वह भी नहीं था। एक प्रत्यय के बाद ही दूसरा प्रत्यय आता है। कार्य के विचार से हम कारण के विचार तक पहुँचते हैं और यदि कार्य नहीं होगा, तो कारण भी नहीं होगा।
|
|||||