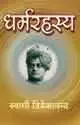|
धर्म एवं दर्शन >> आत्मतत्त्व आत्मतत्त्वस्वामी विवेकानन्द
|
27 पाठक हैं |
आत्मतत्त्व अर्थात् हमारा अपना मूलभूत तत्त्व। स्वामी जी के सरल शब्दों में आत्मतत्त्व की व्याख्या
आधुनिक विज्ञान एवं गणित ज्योतिष (खगोल विद्या) से हमें विदित होता है कि यह पृथ्वी शीतल होती जा रही है और कालान्तर में यह अत्यन्त शीतल हो जायगी, और तब यह खण्ड-खण्ड होकर अधिकाधिक सूक्ष्म होती हुई पुन: आकाश के रूप में परिवर्तित हो जायगी। किन्तु उस सामग्री की रचना के निमित्त, जिससे दूसरी पृथ्वी प्रक्षिप्त होगी, परमाणु विद्यमान रहेंगे। यह प्रक्षिप्त पृथ्वी भी विलुप्त होगी, और फिर दूसरी आविर्भूत होगी। इस प्रकार यह जगत् अपने मूल कारणों में प्रत्यावर्तन करेगा, और उसकी सामग्री संघटित होकर - अवरोह, आरोह करती, आकार ग्रहण करती लहर के सदृश - पुन: आकार ग्रहण करेगी। कारण में बदल कर लौट जाने और फिर पुन: बाहर निकल आने की प्रक्रिया को संस्कृत में क्रमश: 'संकोच और 'विकास' कहते हैं, जिनका अर्थ सिकुड़ना और फैलना होता। इस प्रकार समस्त विश्व संकुचित होता और प्रसार जैसा करता है। आधुनिक विज्ञान के अधिक मान्य शब्दों का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि वह अन्तर्भूत (सन्निहित) और विकसित होता है। तुम विकास के सम्बन्ध में सुनते हो कि किस प्रकार सभी आकार निम्नतर आकारों से विकसित होते हैं और धीरे-धीरे अधिकाधिक विकसित होते रहते हैं। यह बिलकुल ठीक है, लेकिन प्रत्येक विकास के पहले अन्तर्भाव का होना आवश्यक है। हमें यह ज्ञात है कि जगत् में उपलब्ध ऊर्जा का पूर्ण योग सदैव समान रहता है, और भौतिक पदार्थ अविनाशी है। तुम किसी भी प्रकार भौतिक पदार्थ का एक परमाणु भी बाहर नहीं ले जा सकते। न तो तुम थोड़ी भी ऊर्जा कम कर सकते हो और न जोड़ सकते हो। सम्पूर्ण योग सदैव वही रहेगा। संकोचन और विकास के कारण केवल अभिव्यक्ति में अन्तर होता है। इसलिए यह प्रस्तुत चक्र अपने पूर्वगामी चक्र के अन्तर्भाव या संकोचन से प्रसूत विकास का चक्र है। और यह पुन: अन्तर्भूत या संकुचित होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जायगा और उससे फिर दूसरे चक्र का उद्भव होगा। समस्त विश्व इसी क्रम से चल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि का यह अर्थ नहीं कि अभाव से भाव की रचना हुई है। अधिक उपयुक्त शब्द का व्यवहार करें तो हम कहेंगे कि अभिव्यक्ति हो रही है और ईश्वर विश्व को अभिव्यक्त करनेवाला है। यह विश्व मानो उसका नि:श्वास है जो उसी में समाहित हो जाता है और जिसे वह फिर बाहर निकाल देता है।
|
|||||