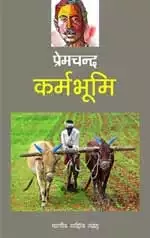|
उपन्यास >> कर्मभूमि (उपन्यास) कर्मभूमि (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
31 पाठक हैं |
प्रेमचन्द्र का आधुनिक उपन्यास…
अपने साथ किसी को न लो, मेरे साथ चलो। मैं ज़िम्मा लेता हूँ कि कोई तुमसे गुस्ताखी न करेगा। उनके जख़्म पर मरहम रख दो, मैं इतना ही चाहता हूँ। जब तक जियेंगे बेचारे तुम्हें याद करेंगे। सद्भाव में सम्मोहन का-सा असर होता है।’
सलीम का हृदय अभी इतना काला न हुआ था कि उस पर कोई रंग ही न चढ़ता। सकुचाता हुआ बोला– ‘मेरी तरफ़ से आप ही को कहना पड़ेगा।
‘हाँ-हाँ, यह सब मैं कर दूँगा; लेकिन ऐसा न हो, मैं उधर चलूँ, इधर तुम हण्टरबाज़ी शुरू करो।’
‘अब ज़्यादा शर्मिन्दा न कीजिए।’
‘तुम तो तजवीज़ क्यों नहीं करते कि असामियों की हालत की जाँच की जाय? आँखें बन्द करके हुक्म मानना तुम्हारा काम नहीं। पहले अपना इत्मीनान तो कर लो कि तुम बेइन्साफ़ी तो नहीं कर रहे हो। तुम ख़ुद ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? मुमकिन है कि हुक्काम इसे पसन्द न करें; लेकिन हक़ के लिए कुछ नुकसान उठाना पड़े, तो क्या चिन्ता।’
सलीम को यह बातें न्यायसंगत जान पड़ीं। खूँटे की पतली नोंक ज़मीन के अन्दर पहुँच चुकी थी। बोला– ‘इस बुजुर्गाना सलाह के लिए आपका एहसानमन्द हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा।’
भोजन का समय आ गया था। सलीम ने पूछा– ‘आपके लिए क्या खाना बनवाऊँ?’
‘जो चाहे बनवाओ; पर इतना याद रक्खो कि मैं हिन्दू हूँ और पुराने ज़माने का आदमी हूँ। अभी तक छूत-छात को मानता हूँ।’
‘आप छूत-छात को अच्छा समझते हैं?’
‘अच्छा तो नहीं समझता; पर मानता हूँ।’
‘तब मानते ही क्यों हैं?’
‘इसलिए कि संस्कारों को मिटाना मुश्किल है। अगर ज़रूरत पड़े, तो मैं तुम्हारा मल उठाकर फेंक दूँगा; लेकिन तुम्हारी थाली में मुझसे न खाया जायेगा।’
‘मैं तो आज आपको अपने साथ बैठाकर खिलाऊँगा।’
|
|||||