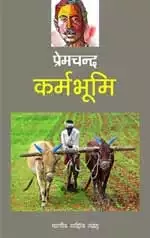|
उपन्यास >> कर्मभूमि (उपन्यास) कर्मभूमि (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
31 पाठक हैं |
प्रेमचन्द्र का आधुनिक उपन्यास…
अमर जैसे गिर पड़ने के बाद गर्द झाड़ता हुआ, प्रसन्नमुख ऊपर चला गया। सुखदा अपने कमरे के द्वार पर खड़ी थी। बोली–‘तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। स्कूल से आकर चरखा ले बैठते हो। क्यों नहीं मुझे घर भेज देते? जब मेरी ज़रूरत समझना, बुला भेजना अबकी आये मुझे छः महीने हुए। मीयाद पूरी हो गयी। अब तो रिहाई हो जानी चाहिए।’
यह कहते हुए उसने एक तश्तरी में कुछ नमकीन और मिठाई लाकर मेज़ पर रख दी और अमर का हाथ पकड़ कमरे में ले जाकर कुरसी पर बैठा दिया।
यह कमरा और सब कमरों से बड़ा, हवादार और सुसज्जित था। दरी का फ़र्श था, उस पर क़रीने से कई गद्देदार और सादी कुर्सियां लगी हुई थीं। बीच में एक छोटी-सी नक्शदार गोल मेज थी। शीशे की आलमारियों में सजिल्द पुस्तकें सजी हुई थीं। आलों पर तरह-तरह के खिलौने रखे हुए थे। एक कोने में मेज़ पर हारमोनियम रखा हुआ था। दीवारों पर धुरन्धर, रवि वर्मा और कई चित्रकारों की तस्वीरें शोभा दे रही थीं। दो-तीन पुराने चित्र भी थे। कमरे की सजावट में सुरुचि और सम्पन्नता का आभास होता था।
अमरकान्त का सुखदा से विवाह हुए दो साल हो चुके थे। सुखदा दो बार तो एक-एक महीना रहकर चली गयी थी। अबकी उसे आये छः महीने हो गये थे; मगर उनका स्नेह अभी तक ऊपर-ही ऊपर था। गहराइयों में दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग थे। सुखदा ने कभी अभाव न जाना था, जीवन की कठिनाइयाँ न सही थीं। वह जाने-माने मार्ग को छोड़कर अनजान रास्ते पर पाँव रखते डरती थी। भोग और विलास को वह जीवन की सबसे मूल्यावान वस्तु समझती थी और उसे हृदय से लगाए रहना चाहती थी। अमरकान्त को वह घर के काम-काज की ओर खींचने का प्रयास करती रहती थी। कभी समझाती थी, कभी रूठती थी, कभी बिगड़ती थी। सास के न रहने से वह एक प्रकार से घर की स्वामिनी हो गयी थी। बाहर के स्वामी लाला समरकान्त थे; पर भीतर का संचालन सुखदा ही के हाथों में था। किन्तु अमरकान्त उसकी बातों को हँसी में टाल देता। उस पर अपना प्रभाव डालने की कभी चेष्टा न करता। उसकी विलासप्रियता मानो खेतों में हौवे की भाँति उसे डराती रहती थी। खेत में हरियाली थी, दाने थे; लेकिन वह हौवा निश्चल भाव से दोनों हाथ फैलाये खड़ा उसकी ओर घूरता रहता था। अपनी आशा और दुराशा, हार और जीत को वह सुखदा से बुराई की भाँति छिपाता था। कभी-कभी उसे घर लौटने में देर हो जाती, तो सुखदा व्यंग्य करने से बाज़ न आती थी–हाँ, यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है! बाहर के मज़े घर में कहाँ! और यह तिरस्कार, किसान की ‘कड़े-कड़े’ की भाँति हौवे के भय को और भी उत्तेजित कर देती थी। वह उसकी खुशामद करता, अपने सिद्धान्तों को लम्बी-से-लम्बी रस्सी देता; पर सुखदा इसे उसकी दुर्बलता समझकर ठुकरा देती थी। वह पति को दया-भाव से देखती थी, उसकी त्यागमय प्रवृत्ति का अनादर न करती थी; पर इसका तथ्य न समझ सकती थी। वह अगर सहानुभूति की भिक्षा माँगता, उसके सहयोग के लिए हाथ फैलाता, तो शायद वह उसकी उपेक्षा न करती। अपनी मुट्ठी बन्द करके, अपनी मिठाई आप खाकर, वह उसे रुला देता। वह भी अपनी मुट्ठी बन्द कर लेती थी और अपनी मिठाई आप खाती थी। दोनों आपस में हँसते-बोलते थे, साहित्य और इतिहास की चर्चा करते थे; लेकिन जीवन के गूढ़ व्यापारों में पृथक् थे। दूध और पानी का मेल नहीं, रेत और पानी का मेल था। जो एक क्षण के लिये मिलकर पृथक् हो जाता था।
|
|||||