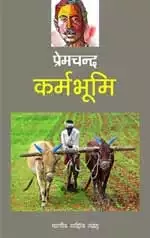|
उपन्यास >> कर्मभूमि (उपन्यास) कर्मभूमि (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
31 पाठक हैं |
प्रेमचन्द्र का आधुनिक उपन्यास…
‘जी नहीं।’
‘आश्चर्य है।’
‘और तो कोई नहीं आया, हाँ वही बदमाश काले खाँ सोने की एक चीज़ बेचने आया था। मैंने लौटा दिया।
समरकान्त की त्योरियाँ बदलीं–‘क्या चीज़ थी?’
‘सोने के कड़े थे। दस तोले बताता था।’
‘तुमने तौला नहीं।’
‘मैंने हाथ से छुआ तक नहीं।’
‘हाँ, क्यों छूते, उसमें पाप लिपटा हुआ था न! कितना माँगता था?’
‘दो सौ।’
‘झूठ बोलते हो।’
‘शुरू दो सौ से किए थे, पर उतरते-उतरते तीस रुपये तक आया था।’
लालाजी की मुद्रा कठोर हो गयी–फिर तुमने लौटा दिए?
‘और क्या करता? मैं तो उसे सेंत में भी न लेता। ऐसा रोज़गार करना मैं पाप समझता हूँ।’
समरकान्त क्रोध से विकृत होकर बोले–‘चुप रहो, शरमाते तो नहीं, ऊपर से बातें बनाते हो। डेढ़ सौ रुपये बैठे-बैठाए मिलते थे, वह तुमने धर्म के घमण्ड में खो दिए, उस पर से अकड़ते हो। जानते भी हो, धर्म है क्या चीज़? साल में एक बार गंगा-स्नान करते हो? एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो? कभी राम का नाम लिया है ज़िन्दगी में?
कभी एकादशी या कोई दूसरा व्रत रखा है? कभी कथा-पुराण पढ़ते या सुनते हो? तुम क्या जानो धर्म किसे कहते हैं। धर्म और चीज़ है, रोजगार और चीज़ छिः, साफ़ डेढ़ सौ फेंक दिए।’
|
|||||